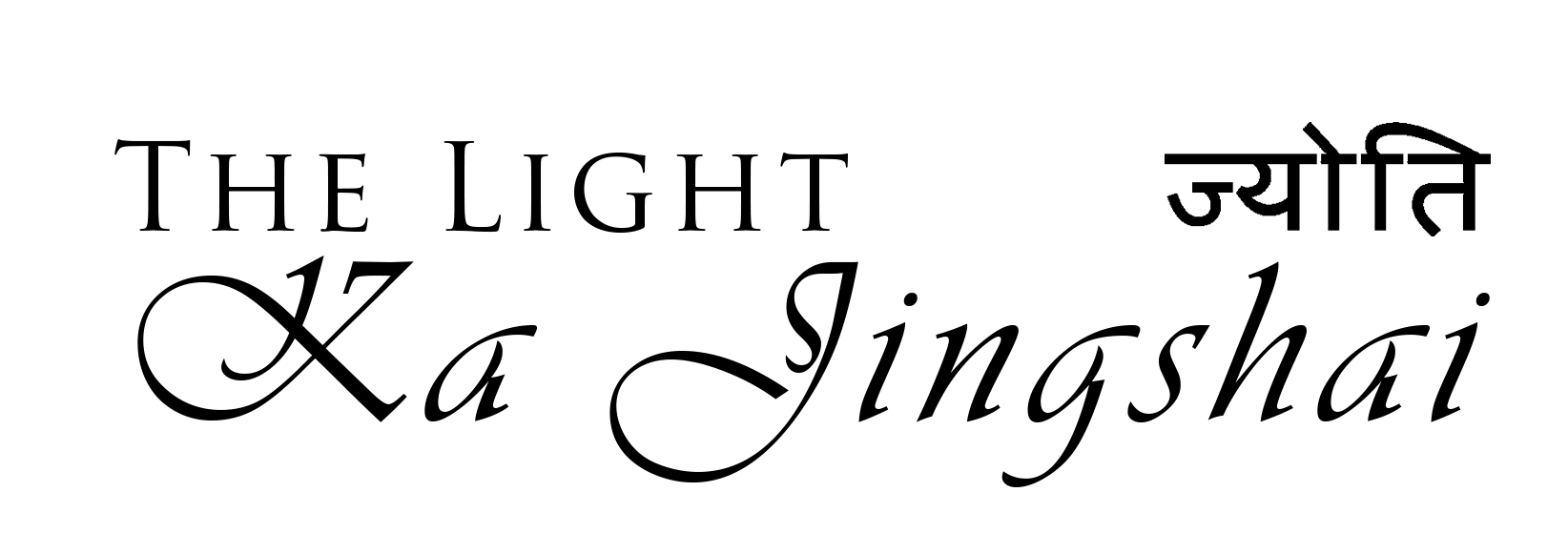अरुणाचल प्रदेश के एक वयोवृद्ध गाँवबुढ़ा से बातचीत हुई और उनके चिंतित स्वर ने हमें झकझोर दिया था। आदी जनजाति के इस जानकार आदमी ने अरुणाचली ज्ञान का समाजशास्त्र और अरुणाचली समाज का ज्ञानशास्त्र समझने हेतु आग्रह किया और उनके महत्त्व को जानने पर बल दिया था। मैं अपनी आईसीएसएसआर-इम्प्रेस टीम के साथ था। अरुणाचली लोक-साहित्य को स्थानीय एवं राष्ट्रीय मीडिया द्वारा यथोचित महत्त्व न दिए जाने के कारण यहाँ की आदिवासी संस्कृति और जनभाषाओं पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों का हम गंभीरतापूर्वक आंकलन कर रहे थे। यह साक्षात्कार इसी परियोजना-कार्य का हिस्सा था और हमारे लिए आँख खोलने वाला था।
इस साल अरुणाचल प्रदेश अपने नामकरण की स्वर्ण-जयंती मना रहा है। आजादी के दो दशक बाद 20 जनवरी, सन् 1972 को अरुणाचल प्रदेश नाम स्वीकृत हुआ। इससे पूर्व यह ‘नार्थ ईस्ट फ्रंट्रियर एजेंसी’ यानी ‘नेफा’ के नाम से जाना जाता था। भारतीय गणराज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी, 1987 ई. को हुई। उत्तर-पूर्व के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में आदिवासी समाज के अलग-अलग समुदाय बसे हुए हैं। उनका रहवास गहरे घाटियों और ऊँचे पहाड़ों के बीच स्थित है। इन जनजातियों की संख्या मुख्य रूप से 26 है जिनकी अपनी ढेरों उप-जनजातियाँ हैं और यह संख्या सौ से भी अधिक हैं। मुख्य जनजातियों में मेयोर, लिसु, अका, बुगुन, वांचो, तांगसा, सिंग्फो, तुत्सा, नोक्ते, मोम्पा, शेरर्दुक्पेन, खाम्ति, मेम्बा, मिजी, न्यीशी, आदी, गालो, तागिन, आपातानी, इदु मिश्मी इत्यादि। यहाँ की नदी-संस्कृति पहाड़ों की जीवनवाहिनी हैं जिसमें सियांग, दिरांग, कामेंग, तिराप, सुबनसिरी, यामने, योमगो, पाचिन, पारे, पापुम, पान्योर, लोहित आदि। इसी तरह याक, ताकिन, मिथुन और धनेश पक्षी के अलावे आर्किड फूल और कीवी फल की प्रचुरता है। होलुङ के पेड़ इस परिक्षेत्र की शोभा है। नाहर एवं अन्य पेड़ खूबसूरत बहुत है। वन-सम्पदा से परिपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में ज्ञात तौर 241 प्रकार के वृ़क्ष होने की पुष्टि एक पुस्तक करती है-‘‘ट्रीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश: अ फील्ड गाइड’। इसी तरह आदी भाषा में ‘तान्नो इलिङ’ कहे जाने वाले फूल की सुन्दरता मोहक है। गणना में 84, 743 वर्ग किलोमीटर में फैला यह प्रदेश प्राकृतिक रूप से जवां और सांस्कृतिक रूप से धनी है। इस प्रदेश में विभिन्न गुणों और प्रचुर उपलब्धता वाले बाँस उपयोगी बहुत है। बम्बू का प्रयोग घर बनाने, खाने से लेकर अपोङ (लोकल दारू) पीने-पिलाने में बहुत होता है। घरों के ऊपर छज्जे के रूप में ‘तोको पत्ता’ का प्रयोग किया जाता रहा है जो आधुनिक दिनों में कम इस्तेमाल हो रहे हैं।
अरुणाचली घर अपनी बनावट एवं संरचना में बेहद आकर्षक मालूम होते हैं जिसे बनाने का काम सारे बस्ती के लोग सामूहिक रूप से करते हैं। आज भी अरुणाचली गाँवों की पहाड़ी खेती में जंगल साफ कर जलाने से लेकर अमुक भूमि पर खेती करने की प्रक्रिया सबलोग मिलजुल कर करते हैं। यह अपनापा और आत्मीयता आदिम जनजाति की बड़ी खूबी है जिसमें सुख और दुःख, खुशी और उदासी सब के सब साझे में मिले-बँटे हुए हैं। इस प्रदेश की बड़ी खूबी भाषिक बहुलता है। जनजातीय भाषा के उच्चार में प्रकृति की अभ्यर्थना और स्तुति सबसे अधिक हैं। इन भाषाओं के शब्द छोटे किन्तु गहरे अर्थ और भावभूमि वाले होते हैं। इनमें एक लय और लोच देखने को मिलते हैं जो मामूली फेरफार के कारण अर्थ-परिवर्तन का कमाल कर डालते हैं। जनजातीय शब्दों की निर्मिति या कहें व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) के नामकरण की रामकहानी अलग है। इन नामों के पीछे का इतिहास परम्परा का अवगाहन करता मालूम देता है। गालो आदिवासी न सिर्फ अपने माता-पिता का नाम जानते हैं, बल्कि अपने 20 पुश्त पहले के पुरखा का नाम भी पता कर लेते हैं जहाँ से उनका खानदान शुरु हुआ है। यह ताज्जुब करने योग्य हो सकता है, किन्तु सचाई यही है कि गालो जनताति में नामकरण की विधि पूर्व-निर्धारित है जिसके माध्यम से नाम रखा जाता है।
अरुणाचली लोक-साहित्य वाचिक परम्परा में अब भी बने हुए हैं। पर्व-त्योहर के अवसर पर इनकी प्रस्तुति पारम्परिक विधि-विधान एवं अनुष्ठान के बीच किया जाता है। इस राज्य को उत्सवप्रिय राज्य कहा जा सकता है जहाँ सालों भर त्योहारों की धूम रहती है। जैसे-सी-दोन्यी, बूरी-बूत, लोसर, तोरग्या, रेह, न्योकुम, मोपिन, सोलुंग, मोह मोल, द्रि, चालो लोकू, आरान, एतोर, खिकसबा इत्यादि। अरुणाचली लोक-साहित्य यहाँ के आदिवासी शब्दों में समोये हुए हैं। इन आदिवासी शब्दों का व्यवहार-जगत में भीतर तक धँसा होना आदिवासीयत की मूल पहचान और जड़ से जुड़ा होना है। अरुणाचली आदिवासी अपने समस्त दुःख-तक़लीफ को शब्दों में रोप देना जानते हैं जिससे निकलने वाले अर्थ गहरी पीड़ा का आकल्पन होती है जिसे बड़ी समझदारी से गाया अथवा स्वरबद्ध किया जाता है। नृत्य का आदिवासी भाषाओं से तालमेल गहरा है। वह युद्ध अथवा उल्लास के लिए भी नृत्य कर अपनी ओजपूर्ण वीरता और प्रसन्नतासूचक उमंग व्यक्त करते हैं। जैसे-तापू नृत्य, बुया नृत्य, रिकमपादा नृत्य, देलोङ नृत्य, पोनुङ नृत्य, पोपिर नृत्य आदि।। ‘सेदी’ और ‘सेलो’ जैसी आदिवासी गाथाएँ हैं जिसमें अनगिन दर्द छुपा हुआ है। अरुणाचली लोक-साहित्य आदिवासी जीवन के दुःख और संत्रास को व्यक्त करने का सघन माध्यम बनते हैं। ‘आंजा’ और ‘पेङे’ शोकगीत यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद गाया जाने वाला स्मरणगीत है जिसे नई पीढ़ी भूलने लगी है।
अरुणाचल प्रदेश की जनभाषाओं में विकल्पन सर्वाधिक है, तो लहजे में बदलाव के कारण उच्चारण में अंतर खूब है। एक ही पहाड की अलग-अलग स्थितियों में रहने वाली समान जनजाति की भाषा में भिन्नता मिलना स्वाभाविक है। यद्यपि पहाड़ों के बीच जीवन सहज नहीं है, तथापि पहाड़ को पैदा होते ही जिन्होंने देखा है; उनसे यारी गाँठी है; दु:ख-सुख, आफत-बिपत सबमें उसी के सुमिरन भरोसे अपने को अब तक बचाए रखा है। वे पहाड़ की परिभाषा नहीं बाँचते। फर्जी नामकरण नहीं करते। दरअसल, पहाड़ उनके लिए सजावटी लैम्प-पोस्ट नहीं है। छवि-निर्माण का तिकड़म या औजार नहीं है। पहाड़ उनके लिए आदिवासीयत-संस्कृति के मजबूत पाँव हैं, जिनसे विलग उनका अपना कोई इतिहास नहीं, सामूहिक-बोध, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक स्मृति नहीं है। जंगल उनकी अपनी दुनिया हैं, तो वनचरों से निकटता और लगाव उनके प्रेम का उत्स। भारतीय आदिवासियों के स्वीकार में दृढ़ता या कहें अटल वचनबद्धता है, तो क्रोध में आवेश का स्फुरण मात्र। उनके यहाँ धोखे की सतरंगी कलाबाजियाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में उन्हें इरादतन सिखाया गया है। उन्हें उनकी ही मूल पहचान से कट जाने की शिक्षा दी जा रही है। उन्हें अपने जड़ और मूल आस्था से जुड़े रहने का आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन अलग-अलग आयातित ‘नेमप्लेट’ के साथ उनके आंतरिक मूल्यों एवं पुरखाई चेतना को नष्ट-विनष्ट भी किया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा-प्रणाली ने इन्हें अपनी मातृभाषा से अधिक दूर कर दिया है या फिर प्रत्यक्ष-परोक्ष बाहरी दबाव एवं आक्रमण के कारण वे अपनी विलुप्त होती जा रही भाषाओं को बचा पाने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश के 25 जिलों में करीब सवा सौ जनजातियाँ हैं जो अपनी भाषा में समृद्ध और सामूहिक चित्तवृत्ति वाली संस्कृति में श्रेष्ठ है। यहाँ गंगा लेक है, जो ताईबिदा की लोककथा आज भी सुनाती है। जयरामपुर, विजयनगर, महादेवपुर, परशुराम कुण्ड, भीष्मकनगर, मालिनीथान, रुक्मिणी मंदिर आदि ऐसे नाम हैं जो उत्तर भारतीय लोक में रचे-बसे द्वापर व त्रेतायुगीन मिथकों की सचाई उजागर कर देते हैं। यह प्रस्थान-बिन्दु भारत की सामासिक-संस्कृति का सच सामने ला कर खड़ा कर देता है। प्राचीनता के ये अवशेष भारतीय सभ्यता के ऐसे स्मारक हैं जिसके समक्ष अखिल भारतीय चेतना मनुष्य मात्र के निमित रची-बुनी गई मालूम पड़ती है। पुरातत्त्व के आधुनिक विशेषज्ञ इस प्रदेश की प्राचीनता को भारत की गौरववर्णी सभ्यता का केन्द्रक मानते हैं। आदिवासियत की बहुआयामी परम्परा और मिथकीय चेतना में अरुणाचल प्रदेश अव्वल है। जीवटता और कर्मठता यहाँ के रहवासियों के गहने हैं। श्रमशीलता उनके जीवन की मुख्य धुरी है। उत्परिवर्तन और उद्वविकास के वे प्राकृतिक यात्री हैं। भाषा में उनके हृदय के फूल खिलते हैं और गंध बिखेरते हैं। कला, शिल्प और नानाविध कौशल भारतीय आदिवासियों का मुख्य श्रृंगार है।
आधुनिक मीडिया तंत्र या कहें संचार विधान में पहाड़ के लिए जगह या तो नहीं है या-है भी तो अल्पमात्र। ऐसे में आदिवासियत को समझने के लिए खुला दिल और सहृदय मन चाहिए। अस्तु, आदिवासी जनसमूह के वाचिक साहित्य को लेकर जिस ढंग की संवेदनशील एवं आत्मिक चेष्टाएँ चाहिए, उसका हर तरफ अभाव है। विशेषतया अरुणाचल या पूर्वोत्तर का आदिवासी लोक-साहित्य मौजूदा विमर्श की केन्द्रीयता एवं पहुँच से बाहर है। अरुणाचली भाषाएँ आज अपनी तमाम खूबियों के बावजूद पहचान के संकट से गुजर रही है। उनके समक्ष अपने को बचाए रखने की चुनौती है। यह घाव नित गहरा होता जा रहा है। मौजूदा मीडिया ने इस घाव को और चोटिल करने का काम किया है। वह बिकाऊ गाय बन चुकी है जिसे दूहते सत्ता-पूँजी के समर्थक हैं। आज की सूचना एवं संचार-संस्कृति में यही गायें भारतीयता के अब तक के हासिल को गोबर करने पर तुली हुई हैं। निःसंदेह वर्तमान मीडिया की सूचना एवं संचार-संस्कृति आलोचना के घेरे में है। यह घेराव पूर्वग्रह या दुराग्रहपूर्ण नहीं है, बल्कि हक़ीकत यही है। वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी मीडिया के वर्ग-चरित्र और वस्तु-स्थिति पर गंभीर टिप्पणी करते हैं कि-“अब मुख्यधारा की मीडिया की स्वतन्त्रता कोरी मिथ है। यह कारपोरेट घरानों व विज्ञापन घरानों का बंधक है। मीडिया सामग्री ‘प्रोडक्ट’ बन चुकी है। यह अब सूचना विचार की वाहक नहीं रही। अतः मीडिया की अन्तर्वस्तु और एकरूपीकृत कार्यशैली सचाई है जो मूल सवालों व मुद्दों का विलोपीकरण या हाशियाकरण करता है तथा सतही सवालों एवं मुद्दों का केन्द्रीकरण करता जाता है।“ परिणास्वरूप मीडिया की मनोगतिकी एवं मनोभाषिकी में अप्रत्याशित फेरफार हुआ है। शब्द अर्थ से आवृत्त न होकर पूँजी के दास हो गए हैं। अब शब्द तक की ‘यूनिक सेलिंग प्राइस’ (यूएसपी) तय की जा रही है। यह देखा जाने लगा है कि ‘शब्द-निवेश’ के कारण माध्यम की प्रभावशीलता में क्या और कितना फ़र्क पड़ रहा है। यह गौरतलब है कि अब छवियों की ही नहीं बल्कि शब्द के अभिविन्यास और उसके सत्ता को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। ये शब्द अर्थ की वजह से नहीं अपनी बिकाऊपन की प्रकृति के कारण प्रयोग में घट या बढ़ रहे हैं। लगातार हाशिए पर धकेली जा रही लोक-संस्कृति और उसके ठेठ लोक-साहित्य को लेकर रोना-धोना मचाने की जगह कुछ बातें ठोस एवं उपयुक्त तरीके से जान लेनी आवश्यक है। आधुनिक सूचनाशास्त्री सुभाष धूलिया का मानना है कि-‘‘समाज के नए-नए तबके मीडिया बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं और अपनी क्रय-शक्ति के आधार पर मीडिया उत्पादों के उपभोक्ता बन रहे हैं। सूचना की इस क्रांति के उपरांत दुनिया में जितने भी संवाद आज हो रहे हैं, वे बेमिसाल हैं; लेकिन इस संवाद का आकार जितना बड़ा है इसकी विषयवस्तु उतनी ही सीमित होती जा रही है। लोग अधिकाधिक मनोरंजित होते जा रहे हैं, और अधिकाधिक कम सूचित/जानकार होते जा रहे हैं।’’
अरुणाचली बौद्धिकों में अपनी ज्ञान-व्यवस्था और सांस्कृतिक कला-शिल्प के प्रति चिंता गाढ़ी हुई है। अपनी भाषाई अस्मिता और पुरखाई कोठार को लेकर वे जागरूक तथा अत्यंत संवेदनशील होते दिखाई दे रहे हैं। शहरी आबोहवा में उनका घरेलूपन जिस तरह छिन्न-भिन्न होता जा रहा है या कि उनकी सामूहिकता की संस्कृति जिस तरीके से अलगाववादी होती जा रही है; वे इसका निषेध करते हुए अपनी अस्मिता और पहचान को ‘पुनि पुनि’ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। परिणामस्वरूप ‘वोकल फॉर लोकल’ की बात तेजी से हो रही है, लेकिन मीडिया की उपेक्षा और इरादतन नज़रअंदाज़ करने का भाव बेचैन कर देता है।
पूर्वकथित गाँवबुढ़ा की चिंता आदी भाषा को लेकर थी। वह नई पीढ़ी के अपनी आदिवासी मूल्य-दर्शन और पहचान-अस्मिता से कटते जाने को लेकर व्यथित थे। माक्तेल परटिन नाम है उनका और पासीघाट से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दाम्बुक गाँव के पोबलुङ बस्ती में रहते हैं। नई पीढ़ी तकनीकी ज्ञान में अव्वल है। उसे झटपट बहुत कुछ करने आता है जिससे आधुनिक जीवन जीना आसान हो चला है। इसे लेकर वह सकारात्मक रूख दिखाते हैं, लेकिन उनकी मूल चिंता भाषा को लेकर है।
अरुणाचल प्रदेश की अधिसंख्य जनजातियाँ अपनी स्वतंत्र लिपि नहीं होने के कारण बड़ी विडम्बना का शिकार है। खाम्पति और मोम्पा आदिवासी के पास लिपि की अपनी परम्परा है, लेकिन उसके जानकार बहुत कम और बेहद विशिष्ट लोग हैं। सामान्य प्रचलन में अरुणाचली लिपि का सर्वथा अभाव है जिस कारण यह प्रदेश दुनिया की दृष्टि में आज भी पूरी तरह से खुला या कि सूचना एवं संचार संस्कृति की सीधी पहुँच में नहीं है। यद्यपि इस दिशा में बहुतेरे प्रयास हुए हैं, तथापि यह नाकाफ़ी है। जैसे-वांचो लिपि, तानी लिपि, गालो लिपि, आदी लिपि आदि। व्यक्तिगत प्रयास द्वारा स्थानीय लिपि-निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन किसी एक लिपि को लेकर अभी अरुणाचल प्रदेश का मानस एकजुट अथवा एकमत नहीं है। लिपि को लेकर जन-स्वीकृति का नहीं होना बड़ी समस्या है। बहरहाल, बहुमान्य लिपि न होने के कारण अरुणाचली जनसमाज अपनी मातृभाषाओं के लोक-साहित्य का संरक्षण एवं संग्रह कर पाने की स्थिति में नहीं है। आकाशवाणी पासीघाट के कार्यक्रम प्रमुख इदाङ परटिन ने बताया कि-‘पासीघाट का यह आकाशवाणी केन्द्र सबसे पुराना केन्द्र है। इस केन्द्र के पास रिकॉर्डेड अति-महत्त्वपूर्ण अभिलेख हैं जो यहाँ के जनसमाज एवं जनसंस्कृति के लिए अमूल्य धरोहर है। लोक-साहित्य आधारित कार्यक्रम की व्यवस्था है। आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें डीआरएम (DRM) और यूपीटीआर (UPTR) की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।”
अरुणाचली प्रसारण में रेडियो की भूमिका अन्यतम रही है। इनके पास मौजूद रिकार्डेड अभिलेख संकटग्रस्त होती जा रही जनजातीय भाषाओं के लिए संजीवनी सरीखा है। ईटानगर स्थित दूरदर्शन के ‘अरुण प्रभा’ चैनल की उल्लेखनीय भूमिका यह रही है कि वह स्थानीय भाषाओं में प्रसारण को लगातार बढ़ावा और मातृभाषाओं में अनेकानेक कार्यक्रम ‘टेलिकास्ट’ कर रहे हैं। यह यूनेस्को के उस रिपोर्ट की चिंता को कम करने की दिशा में ठोस एवं सार्थक पहलकदमी हैं जिसके मुताबिक 1961 ई. की जनगणना में 1652 भाषाओं के होने की जो पुष्टि हुई थी, वह 1971 ई. में मात्र 808 की संख्या में बची थीं। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 2013 ई. में हुए सर्वेक्षण बताते हैं कि पिछले पचास सालों में भारत की 220 भाषाएँ मृत हो चुकी हैं, जबकि 197 भाषाएँ संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। ऐसी दशा में शिक्षा आधारित भाषाई लगाववृत्ति विकसित किया जाना आवश्यक हो चला है। खासकर अरुणाचल प्रदेश की उन भाषाओं के लिए यह खतरा अधिक भयावह है जिसके बोलने वाले की संख्या दो-चार सौ तक सिमट कर रह गई है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के ज्ञानवान समाज और उनकी ज्ञान-संस्कृति का बचाने की मुहिम छेड़ना जरूरी हो गया है। यह और बात है, अरुणाचल प्रदेश की पढ़ी-लिखी पीढ़ी के शौक और स्वप्न तेजी से बदल रहे हैं। वह आदिम आकांक्षा की जन-भावनाओं से भिन्न सोच रही है। वह प्रकृतिजीवी नहीं है, अपितु अधिकाधिक विलासी एवं कृत्रिम जीवन चुन रही है। महँगी गाड़ियों की ख़रीद, बड़े-बड़े बँगलों का शौक तथा सांस्कृतिक उत्पाद एवं उपनिवेश बनते जाना इसका उदाहरण है। ऐसे में अपने समय के अंतर्विरोधों को दर्ज करना है, देशकाल में मौजूद विरोधाभासों से टकराना है तथा अपने समय के द्वंद्वों एवं विडम्बनाओं पर गंभीरता के साथ चिंतन-मनन करना है। जनमाध्यम के लिए ‘मास’ की असल अवधारणा मुख्य भूमिका और औचित्य भी यही है।
- Navendu Page; Aparajita Dutta; Bibidishananda Basu, Trees of Arunachal Pradesh (Mysore:Nature Conservation Foundation, 2022)
- रामशरण जोशी, “असंतोष और असुरक्षा के साये में”, समयांतर (फरवरी, 2011), 8
- समयांतर (फरवरी, 2011) 57
- आईसीएसएसआर-इम्प्रेस क्षेत्र-सर्वेक्षण के अन्तर्गत पासीघाट आकाशवाणी के कार्यक्रम निदेशक इदाङ परटिन द्वारा लिए गए रिकार्डेड साक्षात्कार से।
डॉ. राजीव रंजन प्रसाद राजीव गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं तथा भारतीय समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् द्वारा अनुदानित ‘अरुणाचली लोक-साहित्य और मीडिया: अंतःसम्बन्ध एवं अंतःक्रिया’ शीर्षक शोध-परियोजना कार्य पूर्ण कर चुके हैं।