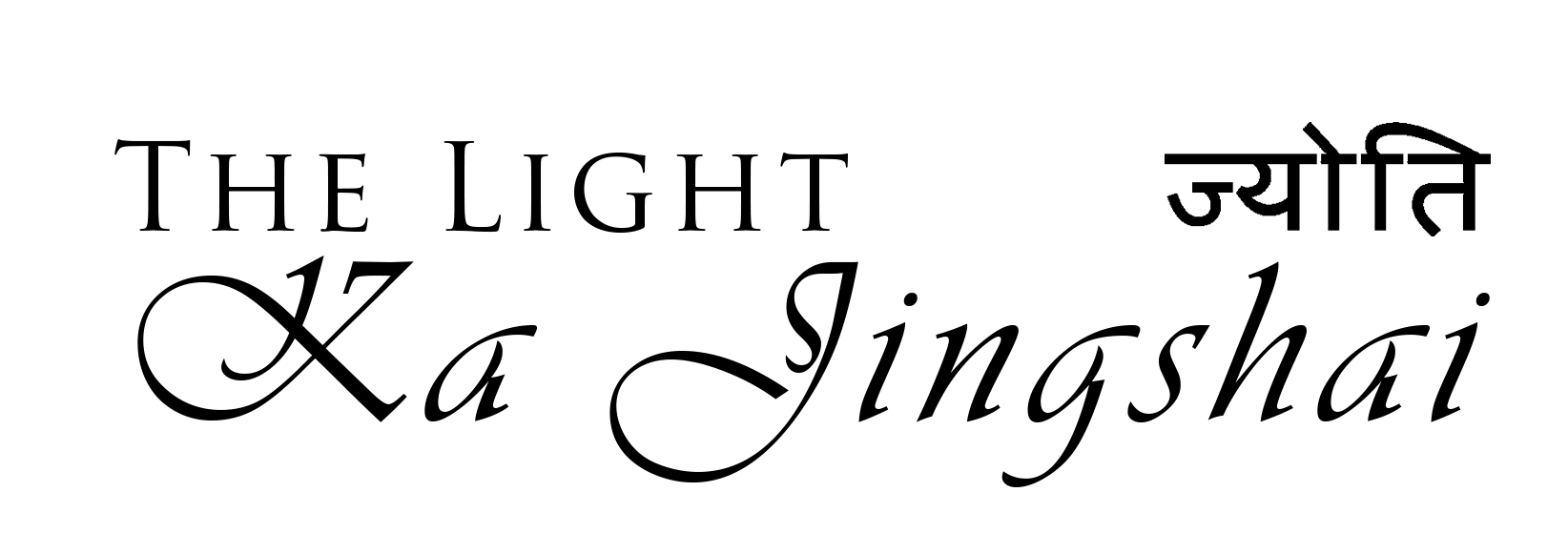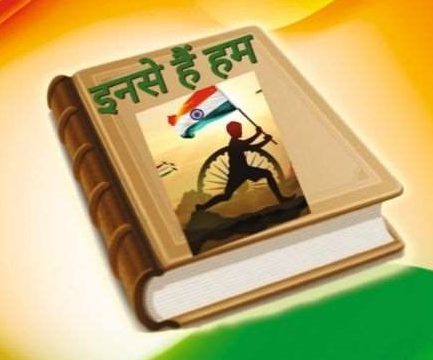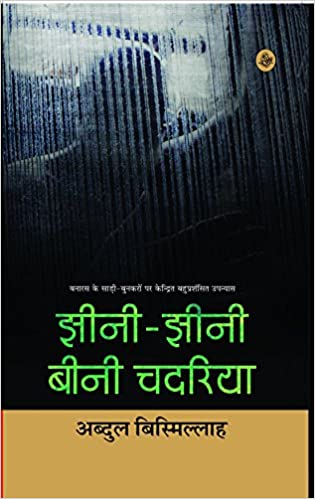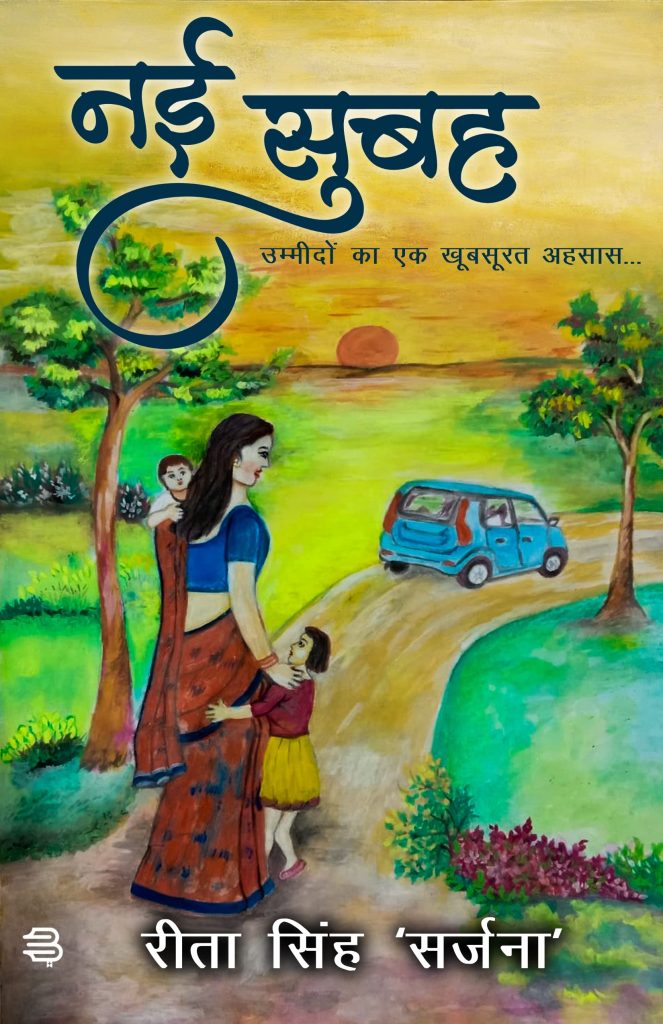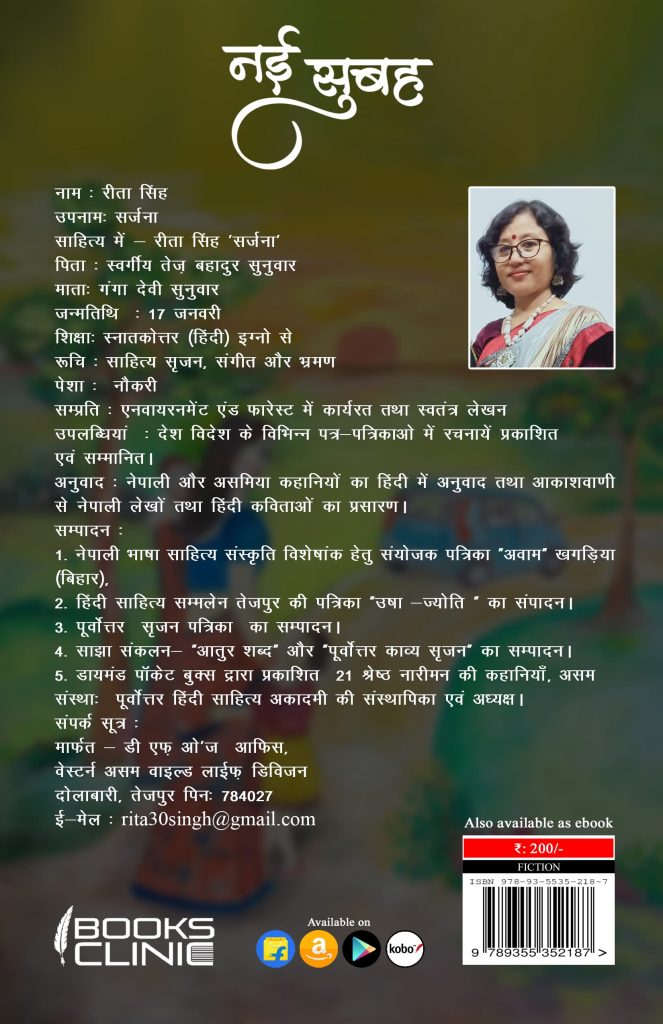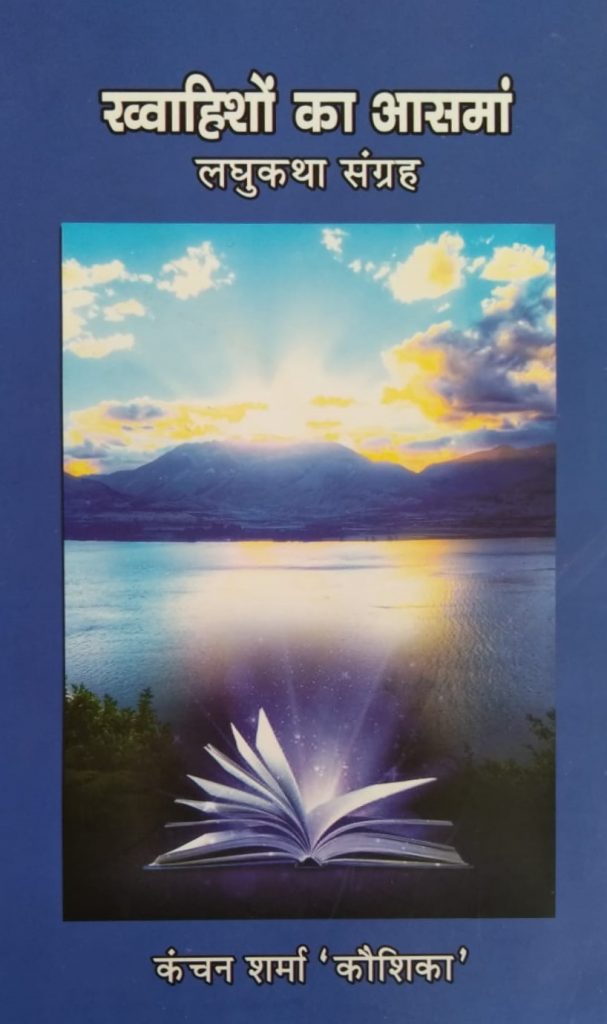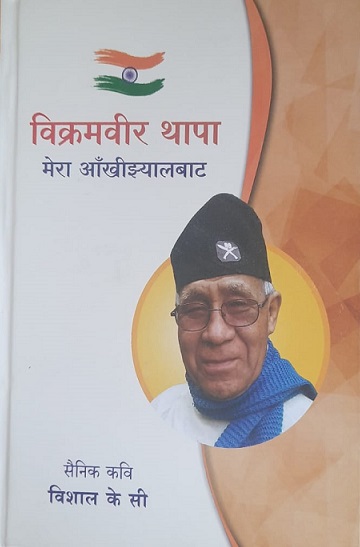पुस्तक -उपनिषदों का संदेश
पुस्तक -उपनिषदों का संदेश
लेखक -स्वामी रंगनाथानन्द
चतुर्थ पुनर्मुद्रण 29- 9 -2017
प्रकाशक- स्वामी ब्रह्मास्थानन्द
धन्तोली( नागपुर )
मूल्य ₹200
ऊँ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते !!
ओम शांति: शांति:
पूर्ण से ही सब कुछ निकला हुआ पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण लेकर भी शेष हमेशा पूर्ण ही रह जाता है। विश्व की परिसीमा में सभ्यता और संस्कृति ने अपनी अस्मिता को कई बार लेखन से, तो कई बार पठन और पाठन से सुरक्षित रखा। भारत देश की सहभागिता को जैसे देवत्व का वरदान है। यह अनोखा देश है, जिसे समय-समय पर आक्रमणकारियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी में ज्ञान संचित रहा।
लेखन प्रथा कब शुरू हुई?इसका पक्का प्रमाण नहीं है। पहले भोजपत्र फिर ताड़ पत्र आगे चलकर मनुष्य के क्रमिक विकास के साथ ,वाचन शैली का रिकॉर्ड होना ,लेखन शैली का प्रिंट मीडिया तक पहुँचना – यह एक प्रकार की क्रमिक व्यवस्था है।मानसिक विकास ने कितनी तरक्की की भला इसका मापक यंत्र कौन बना पाया? देवभूमि भारतवर्ष का मानचित्र भी बदलता गया, कितनी सभ्यताओं, भाषा ,जाति, धर्म की गवाह रही। यह मिट्टी किस-किस तरह के दुख-दर्द का साक्षी बनी। भारतीय धर्म ग्रंथों की महिमा अतुलनीय है। जिसमें महायोगी शिव अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, महापालक विष्णु की कितनी ही कथाएँ वेद, उपनिषद् , कल्प-कल्प, छंद, निरुक्त ,ज्योतिष के ऊपर उनके भेद – प्रभेद चौंसठ कलाओं, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र और लोककार्य अर्थात् जीवन के अनेक संस्कार जन्म से मृत्यु तक वर्णित है।
इनके अनुसार पाँचों तत्व, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, आत्मा स्थिर होकर स्वयं में ही संचरण करती है। उपनिषद् अर्थात् गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करना है। प्रस्तुत ग्रंथ में ईशोपनिषद, कठोपनिषद,केनोपनिषद का सार तत्व आदरणीय स्वामी रंगनाथानन्द जी ने हम साधारण जनों की सुविधा हेतु उपलब्ध कराया है। उपनिषद कहते हैं ‘हे मानव!! तेजस्वी बनो!! दुर्बलता को त्यागो, (विवेकानंद साहित्य पंचम भाग पृष्ठ 132)’
रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के त्रयोदश अध्यक्ष श्रीमद् स्वामी रंगनाथानन्द जी महाराज यह पुस्तक आधुनिक आवश्यकता और आधुनिक चिंतन की दृष्टि से उपनिषदोक्त आत्मतत्व की व्याख्या की है। स्वामी जी ने पुस्तक अंग्रेजी में लिखा ‘द मैसेज ऑफ़ द उपनिषद’।
इस पुस्तक में ईशोपनिषद और केनोपनिषद का हिंदी अनुवाद डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा ने किया और कठोपनिषद का हिंदी अनुवाद आदरणीय श्री ओम बियाणी जी ने किया इसके लिए धन्यवाद ।
‘दूरबोध (टेलीपैथी) का हो सकना कुछ वैज्ञानिक अस्वीकार करते हैं। कहने वालों का तर्क है कि किसी प्रकार की ऊर्जा विनिमय के बिना सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं जा सकती। जैसे हम यदि किसी से कुछ कहें तो शब्द तरंगों और स्नायविक उत्पत्ति के बिना उत्पत्ति के लिए ऊर्जा का प्रयोग करना आवश्यक है। दूरबोध में ऊर्जा-विनिमय के लिए कोई स्थान नहीं है इसलिए दूर-बोध की सत्ता ही नहीं है( पृष्ठ 323) विज्ञान, रास्ते में रुककर संतुष्ट नहीं होता उसका स्वभाव है वह दोनों ही प्रकार के अनुभव वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ को तब तक खोजता है जब तक वह अपने अनुभव का भेद न समझ ले । प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री अरविन श्रोडिंगर कहते हैं, (व्हाट इस लाइफ पृष्ठ 91)’
“चेतना का अनुभव कभी अनेक में नहीं होता है केवल एक में होता है चेतना एक वचन है जिसका बहुवचन अज्ञात है। वह केवल एक ही वस्तु के भिन्न पहलुओं का अनुक्रमण मात्र है, जो वंचना से उत्पन्न होता है। वेदांत की कुछ गूढ़ उक्तियाँ इस साक्षात्कार के चरम बिंदु का प्रकटीकरण हैं।”
सर्वं खलु इदं ब्रह्म (पृष्ठ 331) यह सब विश्व ब्रह्म सर्वसाधारण के लिए ही तो मंत्रों ने स्वयं अपना रूप पिघला लिया है। स्वामीजी ने आसान से आसान शब्दों में प्रस्तुत भी किया है । शब्द, मनिषियों के टोकन मात्र है वह उनके द्वारा हिसाब चुका लेते हैं। संकेत चिन्ह हैं किंतु मूर्खों के लिए वहाँ रुपया है (पृष्ठ 202) केनोपनिषद में कहा गया है(2.4) ‘आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतम——
मनुष्य आत्मा द्वारा महान वीर्य प्राप्त करता है और साक्षात्कार द्वारा अमृततत्व’ (पृष्ठ 202)। वर्तमान में मनुष्य के समक्ष उपलब्धता बढ़ गई है। वह देख नहीं पा रहा है। तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर की सुविधा, वाई-फाई नेटवर्क और ठहरने की व्यवस्था में ही रुचि दिखाती है। ईश्वरमय होना और ईश्वरमय दिखना बहुत ही ज्यादा अंतर है। गणित विषय में ग्राफ का पेपर सभी लोगों के समझ में नहीं आता है, कुछ लोग ही हैं, जो गणित में भी उपदेश और उपदेश में जीवन का गणित समझ पाते हैं। मार्ग हजारों हैं, कहाँ पहुँचना है? पता भी है तो सोचना क्या है?
बुद्धदेव मगध (वर्तमान बिहार) की राजधानी में शिष्यों सहित ठहरे थे। उनका शिष्य थेरा (वरिष्ठ) अस्साजी प्रातः कालीन भिक्षाटन के लिए निकला था। दूसरी एक साधक की टोली है जिसका नायक परम नास्तिक गुरु संजय और सारि पुत्र मुग्गल्लान नामक प्रमुख सदस्य थे। दोनों का व्यक्तित्व अनोखा था और उनके अपने-अपने तर्क भी अनोखे और अकाट्य थे। दोनों ने निश्चित किया था कि जिसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का एहसास हो वह दूसरे को बतायेगा।
उपनिषदों में कठोपनिषद में प्रस्तुत की गई मृत्यु के देवता यम और ऋषि पुत्र नचिकेता के संवाद के बारे में विभिन्न धारणाएँ भी हैं और वह लोगों को बहुत रुचिकर लगती है क्योंकि वह जीवन के कई आयामों से जुड़ा हुआ है। पुत्र अपने पिता से सवाल करता है और पिता यज्ञ-कार्य में व्यस्त है, इसलिए वह बोल देते हैं कि मैं तुम्हें यम को दूँगा। इतना बोलने भर से उनकी आज्ञा को स्वीकार करके नचिकेता बालक का यमराज की खोज में निकल पड़ना, यमराज के साथ मिलना और वहाँ आशीर्वाद के स्वरूप में वरदान प्राप्त करना, ये घटनाएँ घटती हैं। यमराज ने नचिकेता को तीन वरदान दिए साथ ही अपनी तरफ से भी उन्होंने सुंदर रंगों वाली एक माला भी उपहार स्वरूप प्रदान किया और अग्नि विद्या सिखाई, जो नचिकेत अग्नि के नाम से आज भी जानी जाती है। पर जैसे ही नचिकेता आत्मज्ञान की याचना की, यमराज हिचकीचाने लगे। जीवन के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए ग्रंथ का स्वयं अध्ययन कर आस्वादन लेना बहुत जरूरी है।
‘न जातु काम: कामानाम् उपभोगेन् शाम्यति।
हविषा कृष्णवत्मैव भूय एवाभिवर्धते।।
‘भोग द्वारा काम कभी शांत नहीं होते वह उसके द्वारा केवल अधिक प्रज्वलित होते हैं जैसे घृत में अग्नि’( पृष्ठ है 275)
‘श्रेय और प्रेय मुख्य रूप से ज्ञान के दो मार्ग बताए गए हैं’। (पृष्ठ 283)
पृष्ठ -पृष्ठ हम यात्रा करते जाते हैं और अनेक वेद के उद्धरण के साथ विदेशी विद्वानों की पुस्तकों के रहस्य हमारे उपनिषदों की टीकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं। ओंकार जो समस्त सत्य का प्रतीक है, सूचक है।
‘सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति
तपांसि सर्वाणी च यद्वदन्ति
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
त़त्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्
‘सारे वेद जिस लक्ष्य का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधन कहते हैं , जिसकी इच्छा से मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। ऊँ यही वह पद है’( पृष्ठ 360)
शंकराचार्य कहते हैं ऊँ ध्वनि में भी अर्थ निहित है। इसमें इतनी योग्यता है कि गहरे उतरते जाओ, प्रकाशित होकर प्रकाश में समा जाओगे। कई जन्मों का पूर्ण फलता है तो ही अंगुष्ठ मात्र पुरुषोऽन्तरात्मा(पृष्ठ 518) के प्रति कहीं कुछ समर्पण भाव जागृत होता है। स्वामी रंगनाथानन्द जी की ज्ञान शक्ति, अपनी संस्कृति के प्रति भक्ति, समर्पण अतुलनीय है। उन्हें हृदय से प्रणाम।
तूलिका श्री संप्रति- ऑक्जिलियम कन्वट हाई स्कूल, बड़ौदा में हिदी संकृत की अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। इन्हे अखिल भारतीय साहित्यकार अभिनंदन समिति मथुरा द्वारा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मान प्राप्त हैं और बड़ौदा से प्रकाशित हिदी त्रैमासिक पत्रिका नारी अस्मिता में समीक्षक हैं।